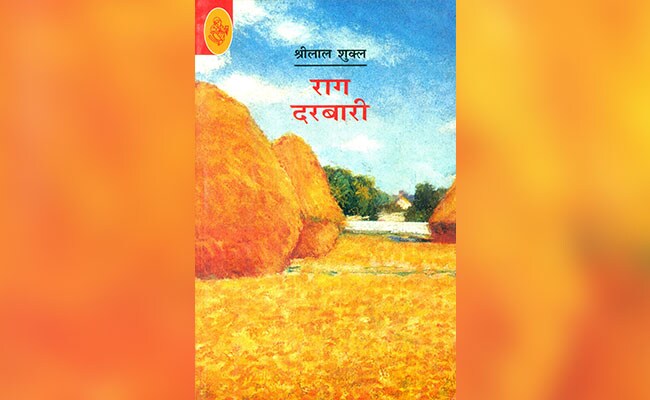
- राग दरबारी का जलवा आज भी कायम है
- धूमिल की कविताएं सत्ता पर करारा प्रहार हैं
- बच्चन की जीवनी कमाल है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:
आजादी के बाद से अब तक का यानी सत्तर साल का समय काफी उथल पुथल भरा समय रहा है. न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी बड़े बदलावों का समय इसे कहा जा सकता है. विभाजन के दंश आजादी के काफी दिनों बाद तक कचोटते रहे हैं. आजादी के इन 70 सालों में दुनिया बेहद बदली है. आजादी मिली तो उसे सम्हालने में हमें वक्त लगा. आजादी के साथ आजादी का मोहभंग कम नहीं रहा. नतीजतन रचनाओं में यह मोहभंग साठ के दशक तक छाया रहा. नेहरू ने भारत के आर्थिक औद्योगिक विकास का जो स्वप्न बुना वह नेहरूवियन माडल के रूप में आलोचना के केंद्र में रहा जहां एक कवि आक्रोश में यह पूछता था, 'आजादी क्या तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है या इसका कोई और मतलब होता है?'
आजादी के समय परिदृश्य में हमारे वक्त के बड़े लेखक मौजूद थे. अज्ञेय, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर, बच्चन, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, आदि जिनके साहित्य ने भारतीय समाज को अपने समय के वैविध्यपूर्ण यथार्थ से जोड़ने का यत्न किया. कविता भी अंतर्मन की खामोश उधेडबुन न होकर समय से सवालों में बदलती गई. रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी, धूमिल, कुंवर नारायण और कैलाश वाजपेयी से होती हुई यह रचनाशीलता केदारनाथ सिंह, जगूड़ी, विनोदकुमार शुक्ल और देवीप्रसाद मिश्र तक हिंदी कविता को अपने नुकीले कथ्य, शिल्प और मुहावरों से संपन्न करती रही है.
यह वह दौर था जब भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता युवाओं के रोमांटिक मिजाज का आईना बन गया था. यशपाल के झूठा सच की आंच बहुतों को दग्ध करती थी. अज्ञेय का नदी के द्वीप चर्चा का विषय बना तो दिनकर की उर्वशी और संस्कृति के चार अध्याय ने साहित्य रसिकों को बहुत आंदोलित किया. मुक्तिबोध इस दौर के सबसे जटिल कवि के रूप में उभरे जिनके संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है और धूमिल के संग्रह संसद से सड़क तक ने कविता की दिशा ही बदल दी. भीष्म साहनी के उपन्यास तमस और राही मासूम रज़ा के आधा गांव ने विभाजन के दंश को बहुत मार्मिक ढंग से उकेरा.
छठे व सातवें दशक के मोहभंग के बाद आपातकाल, भूमंडलीकरण, सांप्रदयिकता के उभार, भ्रष्टाचार व काले धन के घटाटोप और राजनीति में धर्म के संक्रमण ने तेजी से साहित्य को प्रभावित किया है. कांग्रेस के दशकों शासन के बाद गैरकांग्रेसवाद की तेज होती मुहिम और जातीय - धार्मिक ध्रुवीकरण ने क्षेत्रीय दलों और सांप्रदायिक ताकतों को उभरने की जमीन तैयार की. साहित्यिक कृतियों पर इस सबका खासा असर पड़ा है. लेखकों ने अकाल, भुखमरी, संबंधों और मनुष्य में आते दुचित्तेपन को खूबी से अपनी कृतियों में उकेरा है. एक नजर डालते हैं सात दशकों की सात अहम किताबों परः

मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु
आजादी की उत्सवधर्मिता आजादी के बाद धीरे धीरे तिरोहित होने लगी। गांव देहात के विकास की रूपरेखा बनने लगी थी. पर जिस तरह जनता गरीबी रोग अंधविश्वास शोषण आडंबर और राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक हालात से गुजर रही थी कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल में पूर्णिया के मेरीगंज को केंद्र बनाकर स्वातंत्रयोत्तर भारत के पूरब के इस पिछड़े अंचल की एक जीवन्त तस्वीर पेश की है। मैला आंचल ने पहली बार हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की नींव डाली. रेणु कहते थे, ''इसमें फूल भी है, शूल भी है,धूल भी है,गुलाब भी है और कीचड़ भी है. मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया.'' नाटकीयता से भरे 'मैला आँचल’ का नायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी तालीम पूरी करने के बाद पिछड़े गाँव को अपने कार्य-क्षेत्र के रूप में चुनता है, तथा तरह-तरह के सामाजिक शोषण-चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से जुड़ता है. वह बेशक कोई बड़े बदलाव नही ला पाता किन्तु गंवई चेतना में बदलाव की ख्वाहिश जरूर पैदा कर देता है.
राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल
रागदरबारी जाने-माने कथाकार श्रीलाल शुक्ल का ख्यात उपन्यास है जिसके लिये उन्हें 1970 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उपन्यास की किस्सागोई में आदि से अंत तक व्यंग्य की धारावाहिता कायम रहती है. न किस्सागोई बाधित होती है न लेखक का व्यंग्य और विट विराम लेता है। इस उपन्यास के बारे में कुंवर नारायण का कहना है कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने को उस आसान सफलता से बचाया जिसके आकर्षण में रेणु के नक्शेकदम पर चल कर लोगों ने आंचलिक उपन्यासों का अंबार लगा दिया. 1968 में प्रकाशित ‘राग दरबारी' स्वतंत्रता के बाद के भारत के देहाती जीवन की मूल्यहीनता को परत-दर-परत उघाड़ कर रख देने वाला उपन्यास है. जिसकी कथा वस्तु लखनऊ से कुछ दूर शिवपालगंज की है जहाँ प्रगति और विकास की योजनाओं के बावजूद, जीवन और समाज दोनों निहित स्वार्थों और ब्यूरोक्रेसी के आगे लाचार हैं. स्वतंत्रता, न्यायपालिका, पंचायतराज, सहकारिता तथा अन्य संस्थाएं कैसे चंद स्वार्थी ताकतों के हाथो कठपुतली बन कर रह जाती है इसका सच्चा बौर बेबाक नैरेटिव राग दरबारी में दिखता है.
आधा गांव, राही मासूम रजा
हिंदी में राही मासूम रजा अपने अंदाजेबयां से अपना अलग ही मुकाम रखते हैं. उनके उपन्यासों की कथावस्तु व उसकी भाषा में जो प्रवाह और इलाकाई लोच है वह उनके समकालीनों में विरल है. यों तो इससे पहले उनके कई उपन्यास आ चुके थे पर 1966 में प्रकाशित आधा गांव से वे एकाएक चर्चा में आए और उच्च कोटि के उपन्यासकारों में शुमार किए जाने लगे. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास मुस्लिम बहुल गांव गंगौली के इर्द-गिर्द बुने गए कथा संसार के बहाने रजा विभाजन के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों की त्रासदी का महाकाव्यात्मक शब्दांकन करते हैं जिसके बारे में आलोचक वीरेन्द्र यादव का कहना है, 'यह एक उपन्यास भर न होकर उस भारतीय मुसलमान का सामाजिक व राजनीतिक बयान है जो पाकिस्तान के रथ पर आरुढ होने के बजाय उसके पहियों तले लहूलुहान हुआ था.' आधा गाँव विभाजनोत्तर संशयों और चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है.

संसद से सड़क तक. धूमिल
‘साठ के आसपास उभरे अकविता के अराजकतावाद से कविता को मुक्ति दिलाने में धूमिल का योगदान सराहनीय है. यद्यपि उनकी प्रारंभिक कविताओं पर अकविता का झीना प्रभाव रहा है किन्तु 1972 में आए उनके संग्रह संसद से सड़क तक ने हिंदी कविता की दशा दिशा ही बदल दी. पहली बार कविता सामाजिक बदलावों की नियामक की भूमिका में आई. नेहरु युग की विफलताओं व आजादी के मोहभंग ने धूमिल के आक्रोश को कविता की एक नई शब्दावली दी. कविता में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की भूमिका प्रबल हुई. इसमें शामिल पटकथा अपने समय की सचाई का आईना है. कविता को सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य और 'कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है' मानने वाले धूमिल ने अस्पताल में लिखी अपनी आखिरी कविता में लिखा था,' अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो.' मात्र 38 साल की आयु पाने वाले धूमिल ने पटकथा लिख कर लंबी कविता का एक शिखर निर्मित किया जिस यश को कम कवि ही छू सके हैं. लोकतंत्र और आजादी की विफलता का क्रिटीक धूमिल की कविता का केंद्रीय निष्कर्ष रहा है.
चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध
अपने जीवन काल में मुक्तिबोध चांद का मुँह टेढ़ा है का मुँह नहीं देख सके पर इसके प्रकाशन के बाद हिंदी कविता पहली बार एक ऐसे ज्वलंत यथार्थवादी काव्य परिदृश्य से रू-ब-रू हुई जिसने हिंदी कविता को प्रयोगवादी लटके झटकों से दूर जीवन समय और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कवि के उत्तरदायित्व से जोड़ा. मुक्तिबोध के इस संग्रह के बाद अकविता की अराजक मुद्राओं पर विराम लगा और कविता अपने हेतुओं और कसौटियों पर कसी जाने लगी. प्राय: लंबी कविताओं के इस संग्रह में मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताएं संग्रहीत है जिन्होंने कविता की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि को बहुत हद बदलने में कामयाबी पाई है. इस संग्रह की भूमिका शमशेर ने लिखी है. मुक्तिबोध की इन कविताओं में आलोचकों को एक विशाल म्युरल की विशिष्टताएं नज़र आती हैं.
आत्मकथा (चार खंड), हरिवंश राय बच्चन
हिंदी में आत्मकथा बहुतों ने लिखी है किन्तु हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा ने इस अवधारणा को निस्सार कर दिया कि कवि गद्य या आख्यान में पारंगत नहीं होते हैं. पहली बार यह आत्मकथा हिंदी में एक ताजा आबोहवा के रूप में आई तथा जैसा कि गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है, इस कसौटी पर बच्चन सौ फीसदी खरे उतरे. ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ (1969), ‘नीड़ का निर्माण फिर’ (1970), ‘बसेरे से दूर’ (1977) और ‘दशद्वार से सोपान तक’ (1985) चार खंडों की उनकी आत्मकथा इस विधा को नए शिखर पर ले जाती है. इसके पहले खंड में बच्चन जी के बचपन से यौवन तक का वृत्तांत है तो दूसरे खंड में जीवन के बारे में उनका आत्ममंथन बोलता है. तीसरे खंड में बच्चन के विदेश प्रवास का वर्णन है तथा चौथे खंड में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अनुभवों को शब्दबद्ध किया है. कुछ कुछ आत्ममुग्धता में भीगी इस बहुआयामीय आत्मकथा से न केवल बच्चन जी बल्कि उस पूरे युग के साहित्यिक घटनाक्रमों की जानकारी मिल जाती है. भाषा की स्निग्धता का तो कहना ही क्या, वह तो मघई पान की तरह खुशबुओं में भीगी लगती है.

मुझे चांद चाहिए, सुरेन्द्र वर्मा
हिंदी उपन्यासों की विपुल वसुधा में अरसे बाद 1993 में मुझे चांद चाहिए जैसा कोई उपन्यास आया जो शाहजहांपुर जैसे छोटे कस्बे के निम्नमध्यवर्ग परिवार की लड़की यशोदा शर्मा उर्फ सिलबिल की महत्वाकांक्षाओं को एक नई उड़ान देता है जहां वह वर्षा वशिष्ठ बन कर नाटक एवं रंगकर्म की दुनिया एनएसडी से जुड़ कर अभिनय की पायदान पर अपने कदम रखती है और फिर फिल्मी दुनिया में अभिनय की ख्वाहिश में जो कदम चल पड़ते हैं उसके बाद वह पीछे मुड़ कर नहीं देखती. असंभव की आकांक्षा को मन में बसाए वर्षा वशिष्ठ के भीतर प्रेम भी करवटें लेता है और रतिसुख की कौंध भी लुभाती है. निज की पुरातन पारिवारिक बंदिशों को तोड़कर वह तमाम जद्दोजेहद से जो दुनिया अर्जित करती है वह उसके इसी जुनून का नतीजा है जिसे किसी शायर ने यों कहा है: मेरे जुनूँ का नतीजा जरूर निकलेगा. इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा. अपनी नियति और परिवेश से निकल भागने की जो छटपटाहट किसी के मन में होती है वही छटपटाहट वर्षा के भीतर है. भाषा के आभिजात्य के बावजूद अपनी रिकार्ड बिक्री एवं लोकप्रियता के कारण अपने नाटकों से जितनी मकबूलियत सुरेंद्र वर्मा ने नहीं हासिल की उससे ज्यादा ख्याति उन्हे इस उपन्यास ने दिलाई.
डॉ. ओम निश्चल, हिंदी के सुपरिचित कवि, गीतकार, आलोचक हैं.
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.
क्लिक करें: आजादी@70 पर हमारी खास पेशकश
आजादी के समय परिदृश्य में हमारे वक्त के बड़े लेखक मौजूद थे. अज्ञेय, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर, बच्चन, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, आदि जिनके साहित्य ने भारतीय समाज को अपने समय के वैविध्यपूर्ण यथार्थ से जोड़ने का यत्न किया. कविता भी अंतर्मन की खामोश उधेडबुन न होकर समय से सवालों में बदलती गई. रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी, धूमिल, कुंवर नारायण और कैलाश वाजपेयी से होती हुई यह रचनाशीलता केदारनाथ सिंह, जगूड़ी, विनोदकुमार शुक्ल और देवीप्रसाद मिश्र तक हिंदी कविता को अपने नुकीले कथ्य, शिल्प और मुहावरों से संपन्न करती रही है.
यह वह दौर था जब भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता युवाओं के रोमांटिक मिजाज का आईना बन गया था. यशपाल के झूठा सच की आंच बहुतों को दग्ध करती थी. अज्ञेय का नदी के द्वीप चर्चा का विषय बना तो दिनकर की उर्वशी और संस्कृति के चार अध्याय ने साहित्य रसिकों को बहुत आंदोलित किया. मुक्तिबोध इस दौर के सबसे जटिल कवि के रूप में उभरे जिनके संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है और धूमिल के संग्रह संसद से सड़क तक ने कविता की दिशा ही बदल दी. भीष्म साहनी के उपन्यास तमस और राही मासूम रज़ा के आधा गांव ने विभाजन के दंश को बहुत मार्मिक ढंग से उकेरा.
छठे व सातवें दशक के मोहभंग के बाद आपातकाल, भूमंडलीकरण, सांप्रदयिकता के उभार, भ्रष्टाचार व काले धन के घटाटोप और राजनीति में धर्म के संक्रमण ने तेजी से साहित्य को प्रभावित किया है. कांग्रेस के दशकों शासन के बाद गैरकांग्रेसवाद की तेज होती मुहिम और जातीय - धार्मिक ध्रुवीकरण ने क्षेत्रीय दलों और सांप्रदायिक ताकतों को उभरने की जमीन तैयार की. साहित्यिक कृतियों पर इस सबका खासा असर पड़ा है. लेखकों ने अकाल, भुखमरी, संबंधों और मनुष्य में आते दुचित्तेपन को खूबी से अपनी कृतियों में उकेरा है. एक नजर डालते हैं सात दशकों की सात अहम किताबों परः
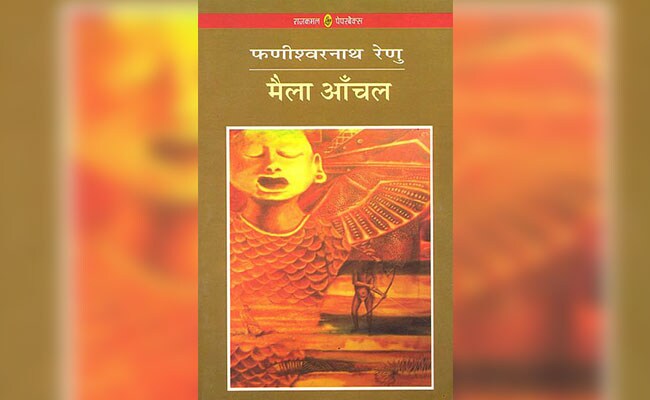
मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु
आजादी की उत्सवधर्मिता आजादी के बाद धीरे धीरे तिरोहित होने लगी। गांव देहात के विकास की रूपरेखा बनने लगी थी. पर जिस तरह जनता गरीबी रोग अंधविश्वास शोषण आडंबर और राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक हालात से गुजर रही थी कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल में पूर्णिया के मेरीगंज को केंद्र बनाकर स्वातंत्रयोत्तर भारत के पूरब के इस पिछड़े अंचल की एक जीवन्त तस्वीर पेश की है। मैला आंचल ने पहली बार हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की नींव डाली. रेणु कहते थे, ''इसमें फूल भी है, शूल भी है,धूल भी है,गुलाब भी है और कीचड़ भी है. मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया.'' नाटकीयता से भरे 'मैला आँचल’ का नायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी तालीम पूरी करने के बाद पिछड़े गाँव को अपने कार्य-क्षेत्र के रूप में चुनता है, तथा तरह-तरह के सामाजिक शोषण-चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से जुड़ता है. वह बेशक कोई बड़े बदलाव नही ला पाता किन्तु गंवई चेतना में बदलाव की ख्वाहिश जरूर पैदा कर देता है.
राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल
रागदरबारी जाने-माने कथाकार श्रीलाल शुक्ल का ख्यात उपन्यास है जिसके लिये उन्हें 1970 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उपन्यास की किस्सागोई में आदि से अंत तक व्यंग्य की धारावाहिता कायम रहती है. न किस्सागोई बाधित होती है न लेखक का व्यंग्य और विट विराम लेता है। इस उपन्यास के बारे में कुंवर नारायण का कहना है कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने को उस आसान सफलता से बचाया जिसके आकर्षण में रेणु के नक्शेकदम पर चल कर लोगों ने आंचलिक उपन्यासों का अंबार लगा दिया. 1968 में प्रकाशित ‘राग दरबारी' स्वतंत्रता के बाद के भारत के देहाती जीवन की मूल्यहीनता को परत-दर-परत उघाड़ कर रख देने वाला उपन्यास है. जिसकी कथा वस्तु लखनऊ से कुछ दूर शिवपालगंज की है जहाँ प्रगति और विकास की योजनाओं के बावजूद, जीवन और समाज दोनों निहित स्वार्थों और ब्यूरोक्रेसी के आगे लाचार हैं. स्वतंत्रता, न्यायपालिका, पंचायतराज, सहकारिता तथा अन्य संस्थाएं कैसे चंद स्वार्थी ताकतों के हाथो कठपुतली बन कर रह जाती है इसका सच्चा बौर बेबाक नैरेटिव राग दरबारी में दिखता है.
आधा गांव, राही मासूम रजा
हिंदी में राही मासूम रजा अपने अंदाजेबयां से अपना अलग ही मुकाम रखते हैं. उनके उपन्यासों की कथावस्तु व उसकी भाषा में जो प्रवाह और इलाकाई लोच है वह उनके समकालीनों में विरल है. यों तो इससे पहले उनके कई उपन्यास आ चुके थे पर 1966 में प्रकाशित आधा गांव से वे एकाएक चर्चा में आए और उच्च कोटि के उपन्यासकारों में शुमार किए जाने लगे. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास मुस्लिम बहुल गांव गंगौली के इर्द-गिर्द बुने गए कथा संसार के बहाने रजा विभाजन के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों की त्रासदी का महाकाव्यात्मक शब्दांकन करते हैं जिसके बारे में आलोचक वीरेन्द्र यादव का कहना है, 'यह एक उपन्यास भर न होकर उस भारतीय मुसलमान का सामाजिक व राजनीतिक बयान है जो पाकिस्तान के रथ पर आरुढ होने के बजाय उसके पहियों तले लहूलुहान हुआ था.' आधा गाँव विभाजनोत्तर संशयों और चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है.
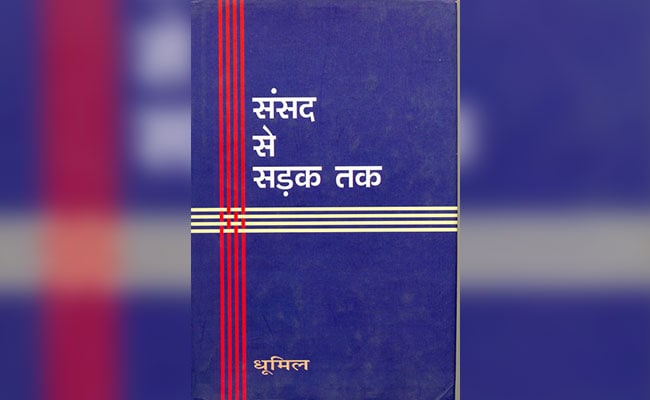
संसद से सड़क तक. धूमिल
‘साठ के आसपास उभरे अकविता के अराजकतावाद से कविता को मुक्ति दिलाने में धूमिल का योगदान सराहनीय है. यद्यपि उनकी प्रारंभिक कविताओं पर अकविता का झीना प्रभाव रहा है किन्तु 1972 में आए उनके संग्रह संसद से सड़क तक ने हिंदी कविता की दशा दिशा ही बदल दी. पहली बार कविता सामाजिक बदलावों की नियामक की भूमिका में आई. नेहरु युग की विफलताओं व आजादी के मोहभंग ने धूमिल के आक्रोश को कविता की एक नई शब्दावली दी. कविता में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की भूमिका प्रबल हुई. इसमें शामिल पटकथा अपने समय की सचाई का आईना है. कविता को सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य और 'कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है' मानने वाले धूमिल ने अस्पताल में लिखी अपनी आखिरी कविता में लिखा था,' अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो.' मात्र 38 साल की आयु पाने वाले धूमिल ने पटकथा लिख कर लंबी कविता का एक शिखर निर्मित किया जिस यश को कम कवि ही छू सके हैं. लोकतंत्र और आजादी की विफलता का क्रिटीक धूमिल की कविता का केंद्रीय निष्कर्ष रहा है.
चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध
अपने जीवन काल में मुक्तिबोध चांद का मुँह टेढ़ा है का मुँह नहीं देख सके पर इसके प्रकाशन के बाद हिंदी कविता पहली बार एक ऐसे ज्वलंत यथार्थवादी काव्य परिदृश्य से रू-ब-रू हुई जिसने हिंदी कविता को प्रयोगवादी लटके झटकों से दूर जीवन समय और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कवि के उत्तरदायित्व से जोड़ा. मुक्तिबोध के इस संग्रह के बाद अकविता की अराजक मुद्राओं पर विराम लगा और कविता अपने हेतुओं और कसौटियों पर कसी जाने लगी. प्राय: लंबी कविताओं के इस संग्रह में मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताएं संग्रहीत है जिन्होंने कविता की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि को बहुत हद बदलने में कामयाबी पाई है. इस संग्रह की भूमिका शमशेर ने लिखी है. मुक्तिबोध की इन कविताओं में आलोचकों को एक विशाल म्युरल की विशिष्टताएं नज़र आती हैं.
आत्मकथा (चार खंड), हरिवंश राय बच्चन
हिंदी में आत्मकथा बहुतों ने लिखी है किन्तु हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा ने इस अवधारणा को निस्सार कर दिया कि कवि गद्य या आख्यान में पारंगत नहीं होते हैं. पहली बार यह आत्मकथा हिंदी में एक ताजा आबोहवा के रूप में आई तथा जैसा कि गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है, इस कसौटी पर बच्चन सौ फीसदी खरे उतरे. ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ (1969), ‘नीड़ का निर्माण फिर’ (1970), ‘बसेरे से दूर’ (1977) और ‘दशद्वार से सोपान तक’ (1985) चार खंडों की उनकी आत्मकथा इस विधा को नए शिखर पर ले जाती है. इसके पहले खंड में बच्चन जी के बचपन से यौवन तक का वृत्तांत है तो दूसरे खंड में जीवन के बारे में उनका आत्ममंथन बोलता है. तीसरे खंड में बच्चन के विदेश प्रवास का वर्णन है तथा चौथे खंड में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अनुभवों को शब्दबद्ध किया है. कुछ कुछ आत्ममुग्धता में भीगी इस बहुआयामीय आत्मकथा से न केवल बच्चन जी बल्कि उस पूरे युग के साहित्यिक घटनाक्रमों की जानकारी मिल जाती है. भाषा की स्निग्धता का तो कहना ही क्या, वह तो मघई पान की तरह खुशबुओं में भीगी लगती है.

मुझे चांद चाहिए, सुरेन्द्र वर्मा
हिंदी उपन्यासों की विपुल वसुधा में अरसे बाद 1993 में मुझे चांद चाहिए जैसा कोई उपन्यास आया जो शाहजहांपुर जैसे छोटे कस्बे के निम्नमध्यवर्ग परिवार की लड़की यशोदा शर्मा उर्फ सिलबिल की महत्वाकांक्षाओं को एक नई उड़ान देता है जहां वह वर्षा वशिष्ठ बन कर नाटक एवं रंगकर्म की दुनिया एनएसडी से जुड़ कर अभिनय की पायदान पर अपने कदम रखती है और फिर फिल्मी दुनिया में अभिनय की ख्वाहिश में जो कदम चल पड़ते हैं उसके बाद वह पीछे मुड़ कर नहीं देखती. असंभव की आकांक्षा को मन में बसाए वर्षा वशिष्ठ के भीतर प्रेम भी करवटें लेता है और रतिसुख की कौंध भी लुभाती है. निज की पुरातन पारिवारिक बंदिशों को तोड़कर वह तमाम जद्दोजेहद से जो दुनिया अर्जित करती है वह उसके इसी जुनून का नतीजा है जिसे किसी शायर ने यों कहा है: मेरे जुनूँ का नतीजा जरूर निकलेगा. इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा. अपनी नियति और परिवेश से निकल भागने की जो छटपटाहट किसी के मन में होती है वही छटपटाहट वर्षा के भीतर है. भाषा के आभिजात्य के बावजूद अपनी रिकार्ड बिक्री एवं लोकप्रियता के कारण अपने नाटकों से जितनी मकबूलियत सुरेंद्र वर्मा ने नहीं हासिल की उससे ज्यादा ख्याति उन्हे इस उपन्यास ने दिलाई.
डॉ. ओम निश्चल, हिंदी के सुपरिचित कवि, गीतकार, आलोचक हैं.
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.
क्लिक करें: आजादी@70 पर हमारी खास पेशकश
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
