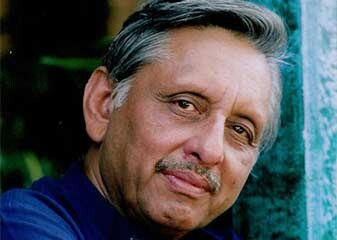
मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य हैं...
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने भारत दौरे के पहले ही दिन भारत को 12 परमाणु रिएक्टर देने की घोषणा की, उसी दिन तेल की कीमतें 60 अमेरिकी डॉलर से भी नीचे आ गईं, और आने वाले दिनों में उसके 35 से 40 डॉलर के बीच पहुंचने की उम्मीद है। इससे यह परमाणु समझौता कम आकर्षक हो गया। इससे यह भी जाहिर होता है कि ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की जगह आणविक ऊर्जा का विकल्प अभी संभव नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में, मोदी को सलाह दी जानी चाहिए कि वह पुतिन से पूछते कि भारत को आणविक सहयोग देने के बजाय रूस भारत को एशियाई गैस और तेल समुदाय के नेटवर्क में शुमार करवाने में किस तरह मदद कर सकता है।
लेकिन चूंकि ऐसी किसी संभावना की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, इसलिए इसे समझाने की जरूरत है। आणविक ऊर्जा अभी भारत की कुल ऊर्जा खपत का महज 1-2 फीसदी हिस्सा मुहैया कराता है, अगर बहुत ज्यादा उम्मीद से भी देखें तो ये आंकड़ा वर्ष 2050 तक भी 6 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ऐसे में हमारी प्राथमिक जरूरत आणविक ऊर्जा नहीं, बल्कि जीवाश्म से मिलने वाली ऊर्जा ही है।
दूसरी बात, जिस तरह से हम कुडनकुलम में देख चुके हैं कि आणविक संयंत्रों के लिए जगह तलाशना हमेशा मुश्किल भरा हो सकता है और यह मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही। अभी कोई भी परमाणु ऊर्जा की मुखालफत नहीं कर रहा है, लेकिन इनमें से हर शख्स अपने आसपास परमाणु संयंत्र लगाने की योजना का विरोध करेगा। हमने ऐसा महाराष्ट्र के जैतापुर और पश्चिम बंगाल में भी देखा है। फुकुशिमा के उदाहरण से यह भी साफ है कि जापान जैसे अति विकसित देश, जहां औद्योगिक विकास की ही संस्कृति है और बेहद अनुशासित वर्क फोर्स है, में भी परमाणु हादसे हो सकते हैं, जिसका असर दशकों तक आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहता है। ऐसे हादसों के सामने भोपाल गैस कांड एक छोटा हादसा नजर आने लगता है।
यही वजह है कि अमेरिका के थ्री माइल द्वीप के परमाणु संयंत्र में 1979 में हुए हादसे के बाद देश के सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया गया, और वे बीते चार दशक से बंद ही पड़े हैं। औद्योगिक रूप से दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में शामिल जर्मनी के पास अपना कोई जीवाश्म ईंधन भी नहीं है, लेकिन उसने फुकुशिमा के हादसे के बाद तय किया कि वह अपने सभी आणविक संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा, और कोई नया संयंत्र नहीं बनाएगा और पूरी तरह जीवाश्म ईंधन और अक्षय ऊर्जा पर निर्भर हो जाएगा। फ्रांस अभी इकलौता देश है, जो परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है, लेकिन उसके पास सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं और अल्जीरिया से पाइपलाइन के जरिये पर्याप्त गैस का भंडार भी, लेकिन भारत जैसे देश के लिए 12 नए रूसी परमाणु संयंत्रों का मतलब मौत के तांडव का खतरा 12 गुना बढ़ने जैसा है।
तीसरी बात, बराक ओबामा यह साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी पर्यावरण में किसी तरह के नुकसान का खतरा देश स्वीकार नहीं करेगा। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में तेल खनन से उपजे संकट के चलते (इसमें किसी इंसान की मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ सील की मौत जरूर हुई थी) 68 अरब डॉलर का हर्जाना भरना पड़ा था। वहीं भारत सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों के प्रभावित होने के बाद भी यूनियन कार्बाइड से महज 480 मिलियन डॉलर का हर्जाना वसूल पाया था। इसके बावजूद, परमाणु दुर्घटना की स्थिति में जबावदेही वाला कानून काफी कठोर माना जा रहा है, वह भी तब, जब एकमात्र अमेरिकी निर्माता कंपनी भारत में आणविक संयंत्र की आपूर्ति कर रही है।
चौथी बात, रूस का परमाणु समझौता उस वक्त सामने आया है, जब पेट्रोलियम के दाम तेजी से कम हो रहे हैं, सो, ऐसे में परमाणु ऊर्जा महंगी दिखने लगी है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि क्यों न दुनिया भर के तेल और गैस की बाज़ार कीमतों में स्थायित्व लाया जाए।
चूंकि रूस प्राकृतिक तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक है, सो, ऐसे में मोदी को पुतिन से रूस से तेल और गैस संसाधनों की आपूर्ति की संभावनाओं के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ऐसा उन्हें दो अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। पहला पहलू तो यही है कि रूस में तेल और गैस संसाधनों का उत्पादन बढ़ने वाला है, क्योंकि पश्चिमी रूस के बदले अब साइबेरियाई फील्ड से इसका उत्पादन बढ़ने जा रहा है। वैसे भी रूसी साइबेरिया को उत्तरी एशिया का हिस्सा मानते हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए था। इतना ही नहीं, साखालिन के जिस द्वीप पर ओएनजीसी और बीपी का प्लांट स्थापित हो रहा है, वह एशिया में स्थित है, यूरोपीय रूस में नहीं।
इतना ही नहीं, रूस का अभी भी पेट्रोलियम सेक्टर पर काफी गहरा असर है, विशेषकर अपने पूर्व संघीय राज्यों पर - कजाकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैज़ान - जिनमें तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन्हीं स्रोतों से चीन अपनी तेल और गैस संबंधी अधिकतर जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है। हमें मध्य और उत्तरी एशियाई में तेल संबंधी कूटनीति में सक्रियता से हिस्सा लेना चाहिए। इसकी संभावना भी बढ़ी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के विवाद के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी ईंधनों का बायकॉट शुरू किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों के चलते भी रूस को विश्वस्त साझीदार तलाशने की जरूरत है और कई बार भरोसे पर खरा उतरे भारत से बेहतर कोई दूसरा साझीदार हो नहीं सकता।
लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि मोदी और पुतिन की बातचीत में पेट्रोलियम तेल पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। सिर्फ परमाणु संयंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर मोदी ने रूस को परमाणु संयंत्रों के एक बड़े बाजार का विकल्प दे दिया है, लेकिन उनसे न सिर्फ हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, देश में परमाणु हादसों का खतरा भी बढ़ेगा।
दरअसल, मोदी के सलाहकारों को पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैसों के जियो-पॉलिटिक्स को समझना होगा। एशिया पेट्रोलियम तेल एवं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। इतना ही नहीं, यह तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे तेजी से बढ़ता बाज़ार भी है, क्योंकि सतत विकास के लिए ईंधन की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके चलते ही, एशियाई पेट्रोलियम और गैस समुदाय बनाने की जरूरत है। इसमें एशियाई गैस ग्रिड की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
भारत के नजरिये से, ऐसे ग्रिड का पहला चरण भारत और ईरान के बीच पाकिस्तान के रास्ते या समुद्र के नीचे की तकनीक के रास्ते का निर्माण है। समुद्र के नीचे का रास्ता भी अब संभव है। ऐसी गैस पाइपलाइन को बाद में कतर और दूसरे खाड़ी देशों तक बढ़ाया जा सकता है। इसे इराक तक ले जाया जा सकता है और एक प्रमुख लाइन को अजरबैजान से जोड़ सकते हैं। पश्चिमी गैस नेटवर्क की तर्ज पर ही हमें तुर्केमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन के निर्माण को गति देनी चाहिए, जिसके लिए सीमा निर्धारण के साथ-साथ जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत है। अगर इन स्रोतों को पूरा किया जाए तो भारत को जरूरत से ज़्यादा तेल और गैस की आपूर्ति संभव होगी। अगर इस पाइपलाइन को म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पश्चिम चीन तक पहुंचाएं तो और भी फायदा होगा। पश्चिमी और मध्य एशियाई गैसों को भारत में लाने के लिए हमें जितना खर्च करना होगा, उससे ज्यादा हम कमा सकते हैं।
इस पैन-एशियाई प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए हमें, टीएपीआई को उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस में कैस्पियन सागर पर स्थित असत्राखान बंदरगाह तक बढ़ाने की जरूरत है। अगर असत्राखान प्रस्तावित एशियाई गैस ग्रिड का हब बनता है तो मध्य एशिया के दूसरे देश इस क्रांतिकारी नेटवर्क से जुड़ने के प्रति ज्यादा आश्वस्त हो पाएंगे।
जहां तक उत्तर एशिया की बात है, साइबेरिया या साखलिन से भारत तक गैस पाइपलाइन तकनीकी तौर पर संभव नहीं दिखती हो, लेकिन भारत और कोरिया और भारत और जापान के बीच दूसरी व्यवस्था संभव है। हम उन्हें उत्तर एशिया के अपने अनुबंधित सेंटर (साखलिन) से गैस की आपूर्ति कर देंगे और उसके बदले हम उनके इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलियाई केंद्र से एलएनजी हासिल कर सकते हैं।
यह सब हासिल करने के लिए, नेहरूवादी नजरिये की जरूरत होगी, जिसे मार्च 1947 में एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस के भारत में आयोजन के साथ नेहरू ने शुरू किया था। तब हम पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हुए थे। प्राचीन काल से ही एशिया दुनिया में मानव सभ्यता के विकास का नेतृत्व करता रहा है, जबकि यूरोप का उपनिवेशवाद महज 300 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन नेहरू की 1947 की पहल के बावजूद एशिया सबसे ज्यादा विभाजित महाद्वीप रहा है। इसकी वजह थी - उपनिवेशवाद के जुए में विकास की राह पर होने के बावजूद एशिया दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए खेल का मैदान बना रहा, खासकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 21वीं शताब्दी में।
यह स्थिति बदलनी ही चाहिए। हमें यूरोप से सबक लेने की जरूरत है। किस तरह उन्होंने पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील समुदाय बनाया, फिर यूरोपियन कॉमन मार्केट, इसके बाद यूरोपीय समुदाय और अब यूरोपियन यूनियन।
हालांकि इस तरह के किसी एशियाई यूनियन की बात अभी एक शताब्दी या उससे भी ज्यादा दूर है, लेकिन हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, और एशियाई गैस ग्रिड की स्थापना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। एशियाई यूनियन के गठन की दिशा में एशियाई तेल एवं प्राकृतिक गैस समुदाय का गठन पहला कदम होगा।
लेकिन भारत यह सब कैसे कर पाएगा, जब वह हिन्दुत्व को बढ़ावा देते हुए हिन्दू राष्ट्र बनना चाहेगा...? ये कैसे हो पाएगा, जब देश की सत्ता का नियंत्रण साक्षी महाराज और साध्वी ज्योति जैसे नेताओं के हाथों में होगा...? क्या हम अपनी विदेश नीति के जनक के सपनों के तहत सभी नजरियों को शामिल करते हुए शुरुआत कर सकते हैं...? ऐसे में बहुत अचरज नहीं होना चाहिए कि मोदी उन परमाणु संयंत्रों को खरीदने को ही प्राथमिकता देंगे, जिसे कोई दूसरा खरीदना नहीं चाहता...
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
