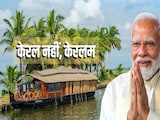भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है. तेज़ विकास की रफ्तार, तकनीक की अंधी दौड़, राजनीतिक आक्रामकता और सांप्रदायिक तनाव – सब मिलकर हमें उस बिंदु पर ले आए हैं जहाँ यह सवाल अनिवार्य हो गया है कि गांधी अब भी हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. क्या गांधी सिर्फ़ सिक्कों, नोटों और स्कूली किताबों तक सिमट गए हैं, या फिर वे हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए उतने ही अपरिहार्य हैं जितने वे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में थे.
गांधी को समझे बिना भारत को समझना असंभव है. गांधी ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को नए सिरे से परिभाषित किया. उन्होंने देखा कि भारत का संकट सिर्फ़ राजनीतिक दासता नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक विभाजन और नैतिक पतन भी है. यही वजह है कि गांधी का दर्शन किसी भी विदेशी सिद्धांत की तुलना में कहीं अधिक भारतीय समाज के वास्तविकताओं के करीब है. पश्चिमी दार्शनिकों ने वर्ग, पूँजी या अनुबंध पर सिद्धांत गढ़े, लेकिन गांधी ने भारत की आत्मा को पढ़ा. यही कारण है कि वे केवल आवश्यक नहीं, बल्कि भारत के लिए अपरिहार्य हैं.
गांधी कैसे भारतीय सोच के मूल में हैं
भारत का समाज न पश्चिमी ढांचों में फिट बैठता है, न किसी एकरेखीय सिद्धांत में. यहां जाति, धर्म, भाषा और भूगोल की असंख्य परतें हैं. गांधी ने इन जटिलताओं को भीतर से समझा और कहा – “मुझे भारत की आत्मा गाँवों में दिखती है.”
उनके लिए गांव केवल भौगोलिक इकाई नहीं थे, बल्कि आत्मनिर्भरता और समानता के प्रतीक थे. यही कारण है कि उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा रखी. उनका मानना था कि भारत तभी मजबूत बनेगा जब गाँव अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम होंगे. आज जब शहरों की भीड़ और उपभोक्तावाद इंसान को थका रहा है, गांधी की यह चेतावनी और भी प्रासंगिक हो उठती है.
असमानता वाले देश मे अहिंसा के अलावा क्या कोई और विकल्प है?
इतिहास गवाह है कि भारत पर बार-बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार इसने अपनी आत्मा बचाए रखी. इतने विशाल और विविध देश को हिंसा से जोड़ना असंभव था. गांधी ने इस सच्चाई को समझा और अहिंसा को केवल रणनीति नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन बनाया.
उनके लिए अहिंसा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत थी. यही वजह है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति बना. इसने पूरी दुनिया को चौंकाया कि बिना हथियार और बिना खून-खराबे के भी साम्राज्यवादी सत्ता को झुकाया जा सकता है. आज जब समाज और राजनीति में असहिष्णुता का बोलबाला है, गांधी का यह दर्शन और भी ज़रूरी हो गया है.
हिन्द स्वराज में गांधी ने लिख दिया था इस सभ्यता की चुनौती
1909 में लिखी गई हिन्द स्वराज गांधी के विचारों का घोषणापत्र कही जा सकती है. इसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को “शैतानी सभ्यता” कहकर चेतावनी दी कि भारत अगर इस अंधी नकल में डूबेगा तो अपनी आत्मा से कट जाएगा.
गांधी ने कहा था कि असली सभ्यता वह है जो इंसान को कर्तव्यों की ओर ले जाए, केवल अधिकारों की ओर नहीं. आज जब प्रगति का पैमाना GDP और उपभोग तक सीमित है, यह प्रश्न और गहरा हो गया है. असली प्रगति क्या है? धन और शक्ति का जमावड़ा या इंसानियत की गहराई?
गांधीवाद क्यों है सरल?
यह सच है कि गांधी के विचार अकादमिक गहराई में रूसो, मार्क्स या लॉक जैसे दार्शनिकों जितने व्यवस्थित नहीं लगते. वे जटिल परिभाषाएं या भारी सिद्धांत नहीं गढ़ते. लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी. गांधी के विचार किताबों की मेज़ से नहीं, बल्कि जीवन की धूल और पसीने से पैदा हुए. उन्होंने जातिगत अन्याय, धार्मिक तनाव, भूगोल की विविधता और आर्थिक शोषण को जनता के अनुभव से पढ़ा. यही वजह है कि उनका दर्शन गूढ़ता से ज़्यादा यथार्थवाद के करीब है. गांधी ने वही कहा जो भारत के लिए ज़रूरी था, न कि वह जो किसी अकादमिक बहस में सुहाना लगता.
चंपारण से दांडी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही तो था
गांधी के विचार केवल किताबों में नहीं रहे, बल्कि आंदोलनों की धूप और धूल में परखे गए. 1917 का चंपारण सत्याग्रह इसका पहला बड़ा प्रमाण था. नील किसानों की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और पहली बार दिखाया कि अहिंसा की ताकत साम्राज्य को झुका सकती है.
1930 का दांडी मार्च इस दर्शन का विस्तार था. गांधी ने नमक कानून तोड़कर सिर्फ़ एक प्रतीकात्मक विद्रोह नहीं किया, बल्कि पूरी ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी. इन आंदोलनों ने साबित किया कि गांधी का दर्शन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहार और प्रयोग की कसौटी पर भी खरा है.
समानता और बंधुत्व ही तो गांधी की ताकत थी
गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति का संघर्ष नहीं बनाया. उन्होंने इसे सामाजिक सुधार की प्रक्रिया भी बनाया. अस्पृश्यता को उन्होंने “पाप” कहा और हरिजन आंदोलन शुरू किया.
उनकी राजनीति सत्ता की भूख पर नहीं, बल्कि सेवा और नैतिकता पर आधारित थी. गांधी ने कहा था – “मेरी राजनीति का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है, यह सत्य और अहिंसा से प्रेरित है.” आज जब राजनीति सत्ता के खेल में बदल गई है, गांधी की यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा को याद दिलाती है.
ट्रस्टीशिप का मॉडल: पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता
भारत जैसे गहरी असमानताओं वाले समाज के लिए गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया. उनका विश्वास था कि अमीर वर्ग अपनी संपत्ति को समाज की सेवा के लिए ट्रस्ट की तरह माने. उनका कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है
- महात्मा गांधी
उनका स्वदेशी आंदोलन भी इसी सोच का हिस्सा था. खादी और चरखा उनके लिए प्रतीक मात्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी थे. आज का वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया उसी सोच का आधुनिक संस्करण है.
गांधी ने समस्या के जड़ पर हमेशा चोट किया
भारत का सबसे बड़ा संकट हमेशा सांप्रदायिकता रहा है. गांधी ने इसे गहराई से समझा और कहा- “मेरा धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है.” उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए अपने जीवन की बाज़ी लगा दी. अंततः उनकी हत्या भी इसी नफ़रत का परिणाम बनी. लेकिन उनकी शहादत ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत केवल तभी जीवित रह सकता है जब इंसानियत धर्म से ऊपर रहे.
बुद्ध के बाद गांधी ही थे जिसके सामने झुक गई दुनिया
गांधी का दर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि “प्रेम हमें ईसा से मिला, पर गांधी ने सिखाया कि इसे जीवन में कैसे उतारें.” नेल्सन मंडेला ने माना कि दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेद विरोधी लड़ाई में गांधी उनके मार्गदर्शक थे. यह बताता है कि गांधी का विचार मानवता की साझा धरोहर है, केवल भारत की संपत्ति नहीं.
भारत आज असमानता, सांप्रदायिक तनाव, पर्यावरण संकट और राजनीति के केंद्रीकरण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है. गांधी का ट्रस्टीशिप, स्वदेशी और अहिंसा आज भी हमें समाधान का रास्ता दिखाते हैं. गांधी कोई अकादमिक सिद्धांतकार नहीं थे, बल्कि भारतीय आत्मा के व्याख्याकार थे. उनका हिन्द स्वराज केवल किताब नहीं, बल्कि चेतावनी थी कि अगर भारत अपनी आत्मा से कटेगा तो खो जाएगा. विंस्टन चर्चिल ने कहा था – “गांधी मर सकते हैं, उनके शरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन उनके विचार अमर रहेंगे.” यही कारण है कि आज भी, जब भारत अपनी राह खोज रहा है, गांधी केवल आवश्यक नहीं, बल्कि अपरिहार्य हैं.
सचिन झा शेखर NDTV में कार्यरत हैं. राजनीति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर लिखते रहे हैं.
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.